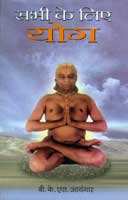|
योग >> सभी के लिए योग सभी के लिए योगबी. के. एस. आयंगारएस पी गौतमदेवीप्रसाद मिश्रासमीर
|
147 पाठक हैं |
||||||||
योग-साधना के विश्वविख्यात उपासक एवं योगाचार्य बी.के.एस. आयंगार द्वारा योग विषय पर हिन्दी में प्रकाशित पहली पुस्तक।
Sabhi Ke Liye Yog
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
योग-साधना के विश्वविख्यात उपासक एवं योगाचार्य बी.के.एस. आयंगार द्वारा योग विषय पर हिन्दी में प्रकाशित पहली पुस्तक। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि योग जैसे विस्तृत विषय पर लिखित यह पुस्तक परंपरा से हटकर है।
इसमें योगासनों के विशुद्ध रूप, उनका शुद्धाचरण, उनकी बारीकियाँ, शरीर की कमियाँ और रोग-व्याधियों के अनुसार योगासनों का चयन आदि के सम्बन्ध में सविस्तार मार्गदर्शन सहज, सरल एवं बोधगम्य रूप में किया गया है। योग और योगासनों का सूक्ष्म विश्लेषण, जो हर आयु-वर्ग के पाठकों हेतु उपयोगी है।
अधिक विस्तृत एवं उपयोगी जानकारियाँ, जिन्हें पढ़कर पाठकगण आसानी से योग, योगासन व प्राणायाम सीख सकते हैं। विशिष्ट संप्रेषण शैली एवं शरीर विज्ञान सम्बन्धी वैज्ञानिक विश्लेषण पुस्तक की अतिरिक्त विशेषता है। योगासनों की विभिन्न स्थितियों को दरशाते लगभग 300 रेखाचित्र, ताकि विषय को समझने में आसानी रहे। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि अंगों के सर्वांगीण विवेचन से परिपूर्ण पुस्तक।
प्रत्येक परिवार के लिए पठनीय, उपयोगी एवं संग्रहणीय पुस्तक।
इसमें योगासनों के विशुद्ध रूप, उनका शुद्धाचरण, उनकी बारीकियाँ, शरीर की कमियाँ और रोग-व्याधियों के अनुसार योगासनों का चयन आदि के सम्बन्ध में सविस्तार मार्गदर्शन सहज, सरल एवं बोधगम्य रूप में किया गया है। योग और योगासनों का सूक्ष्म विश्लेषण, जो हर आयु-वर्ग के पाठकों हेतु उपयोगी है।
अधिक विस्तृत एवं उपयोगी जानकारियाँ, जिन्हें पढ़कर पाठकगण आसानी से योग, योगासन व प्राणायाम सीख सकते हैं। विशिष्ट संप्रेषण शैली एवं शरीर विज्ञान सम्बन्धी वैज्ञानिक विश्लेषण पुस्तक की अतिरिक्त विशेषता है। योगासनों की विभिन्न स्थितियों को दरशाते लगभग 300 रेखाचित्र, ताकि विषय को समझने में आसानी रहे। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि अंगों के सर्वांगीण विवेचन से परिपूर्ण पुस्तक।
प्रत्येक परिवार के लिए पठनीय, उपयोगी एवं संग्रहणीय पुस्तक।
पतंजलि की प्रार्थना
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शारीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पर जलिं प्रा जलिरानतोऽस्मि।।
आबाहु पुरुषाकारं शंखचक्रासि धारिणम्।
सहस्र शिरसं भवेत प्रणमामि पतं जलिम्।।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पर जलिं प्रा जलिरानतोऽस्मि।।
आबाहु पुरुषाकारं शंखचक्रासि धारिणम्।
सहस्र शिरसं भवेत प्रणमामि पतं जलिम्।।
अर्थात् चित्त शुद्धि के लिए योग, वाणी-शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर-शुद्धि के लिए वैद्यकशास्त्र देनेवाले मुनिश्रेष्ठ पातंजलि को प्रणाम ! जिनकी ऊर्ध्व देह मनुष्याकार है, जिन्होंने हाथ में शंक, चक्र और तलवार धारण की है, उन सहस्रशीर्ष आदिशेषावतार पातंजलि को प्रणाम !
लेखक का मनोगत
पुणे ‘सकाळ’ दैनिक संपादक कै.ना.भि. परुळेकर से मेरा कई वर्षों से परिचय था। उस पृष्ठभूमि में मित्रता की स्मृतियों को ताजा करते हुए ‘सकाळ’ संस्था की ओर से वर्तमान संपादक श्री विजय कुवळेकर द्वारा ‘रविवार सकाळ’ में योग-साधना पर वर्ष भर लेखमालिका लिखने के लिए मेरे पास प्रस्ताव आया। अस्सी वर्ष की आयु पूरी करते समय अर्थात् सहस्रचंद्रदर्शन होते समय अपनी पाँच तप से अधिक योग साधना को, पतंजलि के योग दर्शन को यदि मैं पूर्ण स्वास्थ्य के लिए व्यावहारिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक प्रस्तुत कर सकूँ तो स्वयं को कृतार्थ समझूँगा और समाज के ऋण से, अंशतः ही क्यों न हो, उऋण हो सकूँगा। इसलिए अवसर को न खोकर मैंने उक्त लेखमाला लिखना स्वीकार कर लिया । उसी का परिणाम है यह पुस्तक।
किसी भी विषय को शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को दूसरे देश में भोजन करना हो तो स्वाद न लिये हुए पदार्थ को चखने की उसमें अजीब सी उत्सुकता होती है। पहले क्या खाया जाए और अंत में क्या खाया जाए या किसके साथ क्या खाना है तथा किसमें क्या मिलाना है आदि उसे समझ में नहीं आता। परंतु नाक से आनेवाली गंध और जिह्वा के स्वाद से यदि वह उस पदार्थ का आस्वाद लेगा तो उसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है; बल्कि उस नए व्यक्ति के लिए यही आसान व सरल-सुगम मार्ग है।
नौसिखियों को योगविद्या का आस्वाद भी ऐसे ही लेना पड़ता है। जो सुगम और सुसाध्य है, उसे पहले लेना चाहिए। अर्थात् अष्टांग योग की सीढ़ियाँ नहीं होतीं। यह योग अष्टदल होता है। गुलाब के सुंदर फूल की ओर हम सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। योग के अष्टांग भी गुलाब की पंखुड़ियों की भाँति हैं। लेकिन फूलों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर लगता है कि सभी पँखुड़ियाँ एक स्तर पर न होकर अलग-अलग स्तर पर होती हैं। बाहर और अंदर की पँखुड़ियों का आकार स्थूल रूप से एक जैसा लगता है, पर अंदर की पँखुड़ियाँ तुलनात्मक दृष्टि से सूक्ष्मतर होती जाती हैं। अष्टांग योग का पुष्प भी ऐसा ही है। प्रथम दृष्टि में जो आकलनीय है, उसे लेना पड़ता है। यह सही है कि यम-नियमों का परिपालन सूक्ष्मता से और अनुशासन से करना असंभव होता है। यह सब करने के लिए परिस्थितियों में बदलाव लाना पड़ता है, बल्कि मनःस्थिति में भी बदलाव लाना आवश्यक है।
चित्त को उच्च स्तर पर ले जाना पड़ता है। आसन-प्राणायाम का भी वैसा ही है। व्याधि-पीड़ित मनुष्य को स्वास्थ्य, आरोग्य का आकर्षण आंतरिक होता है, क्योंकि वह उसकी जरूरत होती है।’ पर जरूरत पूरी हो जाने पर वैद्यकीय उपचार के स्तर से आत्मविद्या के स्तर पर जाने का दायित्व भी उसका अपना होता है। जीवन भोजन के लिए नहीं बल्कि भोजन जीवन के लिए है, इसे ध्यान में रखना पड़ता है। आसन-प्राणायम के अभ्यास की बारीकियों को सीखने एवं आत्सात् करने के लिए मूर्त से अमूर्त की ओर अंतर्यात्रा शुरू हो जाती है। उसे प्रत्याहार सहित नए स्तर का एहसास होने लगता है। शरीर के अंदर का प्रत्येक स्थान आत्मस्थान है। उसे चेतनाशक्ति से आविर्भूत, प्राणशक्ति से पूरित (परिपूर्ण) और आत्मशक्ति से व्याप्त अंतर का—प्रकाशित चित्त के कारण—अनुभव होने लगता है। उससे ही उसे ध्यान-धारणा की ओर जाने का मार्ग मिल जाते है।
प्रस्तुत पुस्तक लेखन का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य के लिए योग का अनुसरण कैसे किया जाए, होने पर भी मेरे अंदर रचे-बसे साधक और पूर्ण स्वरूप में वर्णित करके पाठकों तक पहुँचाने का एक विनम्र प्रयास है। हो सकता है, यह सबके लिए सुगम न हो, लेकिन मेरे अंतरतम का मनोयोग एवं लगन उनके ध्यान में अवश्य आएगी।
छात्रवर्ग ने मुझे भाषा के संदर्भ में तथा चित्रकला के जानकार व्यक्तियों ने रेखाचित्र बनाने के संदर्भ में जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। पुस्तक को सरल व सुगम बनाने में अपने संपादन के कार्य से बहुमूल्य योगदान देकर श्री पुरुषोत्तम धाक्रस ने जो सहायता की, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ।
डॉ. दुर्गा दीक्षित ने पुस्तक के हिंदी रूपांतरण का जटिल कार्य सुचारु रूप से पूरा किया तथा इस कार्य में सुश्री निवेदिता जोशी ने उनकी सहायता की। हिंदी रूपांतरण के माध्यम से ‘सभी के लिए योग’ पुस्तक हिंदी भाषी पाठकों के लिए उपलब्ध कराने के बहुमूल्य कार्य में सहयोग के लिए इन दोनों का मैं आभारी हूँ। पाठकों के हाथों में यह पुस्तक सौंपते हुए यह सदिच्छा, कि उनका योग संबंधी ज्ञान क्षितिज अधिकाधिक व्यापक होता जाए, रखते हुए परमात्मा के श्रीचरणों में यह पुस्तक समर्पित करता हूँ।
किसी भी विषय को शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को दूसरे देश में भोजन करना हो तो स्वाद न लिये हुए पदार्थ को चखने की उसमें अजीब सी उत्सुकता होती है। पहले क्या खाया जाए और अंत में क्या खाया जाए या किसके साथ क्या खाना है तथा किसमें क्या मिलाना है आदि उसे समझ में नहीं आता। परंतु नाक से आनेवाली गंध और जिह्वा के स्वाद से यदि वह उस पदार्थ का आस्वाद लेगा तो उसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है; बल्कि उस नए व्यक्ति के लिए यही आसान व सरल-सुगम मार्ग है।
नौसिखियों को योगविद्या का आस्वाद भी ऐसे ही लेना पड़ता है। जो सुगम और सुसाध्य है, उसे पहले लेना चाहिए। अर्थात् अष्टांग योग की सीढ़ियाँ नहीं होतीं। यह योग अष्टदल होता है। गुलाब के सुंदर फूल की ओर हम सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। योग के अष्टांग भी गुलाब की पंखुड़ियों की भाँति हैं। लेकिन फूलों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर लगता है कि सभी पँखुड़ियाँ एक स्तर पर न होकर अलग-अलग स्तर पर होती हैं। बाहर और अंदर की पँखुड़ियों का आकार स्थूल रूप से एक जैसा लगता है, पर अंदर की पँखुड़ियाँ तुलनात्मक दृष्टि से सूक्ष्मतर होती जाती हैं। अष्टांग योग का पुष्प भी ऐसा ही है। प्रथम दृष्टि में जो आकलनीय है, उसे लेना पड़ता है। यह सही है कि यम-नियमों का परिपालन सूक्ष्मता से और अनुशासन से करना असंभव होता है। यह सब करने के लिए परिस्थितियों में बदलाव लाना पड़ता है, बल्कि मनःस्थिति में भी बदलाव लाना आवश्यक है।
चित्त को उच्च स्तर पर ले जाना पड़ता है। आसन-प्राणायाम का भी वैसा ही है। व्याधि-पीड़ित मनुष्य को स्वास्थ्य, आरोग्य का आकर्षण आंतरिक होता है, क्योंकि वह उसकी जरूरत होती है।’ पर जरूरत पूरी हो जाने पर वैद्यकीय उपचार के स्तर से आत्मविद्या के स्तर पर जाने का दायित्व भी उसका अपना होता है। जीवन भोजन के लिए नहीं बल्कि भोजन जीवन के लिए है, इसे ध्यान में रखना पड़ता है। आसन-प्राणायम के अभ्यास की बारीकियों को सीखने एवं आत्सात् करने के लिए मूर्त से अमूर्त की ओर अंतर्यात्रा शुरू हो जाती है। उसे प्रत्याहार सहित नए स्तर का एहसास होने लगता है। शरीर के अंदर का प्रत्येक स्थान आत्मस्थान है। उसे चेतनाशक्ति से आविर्भूत, प्राणशक्ति से पूरित (परिपूर्ण) और आत्मशक्ति से व्याप्त अंतर का—प्रकाशित चित्त के कारण—अनुभव होने लगता है। उससे ही उसे ध्यान-धारणा की ओर जाने का मार्ग मिल जाते है।
प्रस्तुत पुस्तक लेखन का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य के लिए योग का अनुसरण कैसे किया जाए, होने पर भी मेरे अंदर रचे-बसे साधक और पूर्ण स्वरूप में वर्णित करके पाठकों तक पहुँचाने का एक विनम्र प्रयास है। हो सकता है, यह सबके लिए सुगम न हो, लेकिन मेरे अंतरतम का मनोयोग एवं लगन उनके ध्यान में अवश्य आएगी।
छात्रवर्ग ने मुझे भाषा के संदर्भ में तथा चित्रकला के जानकार व्यक्तियों ने रेखाचित्र बनाने के संदर्भ में जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। पुस्तक को सरल व सुगम बनाने में अपने संपादन के कार्य से बहुमूल्य योगदान देकर श्री पुरुषोत्तम धाक्रस ने जो सहायता की, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ।
डॉ. दुर्गा दीक्षित ने पुस्तक के हिंदी रूपांतरण का जटिल कार्य सुचारु रूप से पूरा किया तथा इस कार्य में सुश्री निवेदिता जोशी ने उनकी सहायता की। हिंदी रूपांतरण के माध्यम से ‘सभी के लिए योग’ पुस्तक हिंदी भाषी पाठकों के लिए उपलब्ध कराने के बहुमूल्य कार्य में सहयोग के लिए इन दोनों का मैं आभारी हूँ। पाठकों के हाथों में यह पुस्तक सौंपते हुए यह सदिच्छा, कि उनका योग संबंधी ज्ञान क्षितिज अधिकाधिक व्यापक होता जाए, रखते हुए परमात्मा के श्रीचरणों में यह पुस्तक समर्पित करता हूँ।
-बी.के.एस. आयंगर
सर्वस्पर्शी साधना
भारतीय संस्कृति में योग विद्या का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन को स्पष्ट करने वाले छह दर्शनों में से एक दर्शन है योग। ‘योगशास्त्र’ बहुत प्राचीन शास्त्र है। ऐसा विश्वास है कि यह स्वयं ब्रह्मा के द्वारा मानव जाति को दिया हुआ वरदान है। महर्षि पतंजलि ने ईसा से दो सौ वर्ष पहले योग-साधना की रचना सूत्र के रूप में की थी। उनके पूर्व योग विषयक जानकारी कई वेद ग्रंथों में कहीं-कहीं बिखरे रूप में अवश्य थी। बाद के काल में उपनिषद् संहिता, हठयोग-प्रदीपिका, घेरंडसंहिता, शिवसंहिता जैसे अलग-अलग ग्रंथों में उसका विस्तार पाया जाता है। समय के अनुसार विषयों में परिवर्तन होते रहे, लेकिन योग मूलताः बुद्धिनिष्ठ ही रहा।
इस शास्त्र में मानव में शारीरिक, मानसिक नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन करने की शक्ति तो है, साथ ही उसके अपने व्यक्तिगत सांस्कृतिक स्तर और पूरे समाज के सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने की क्षमता भी है। इसीलिए तो यह शास्त्र मानव जाति के लिए वरदान है। पिछली आधी शती में जनसामान्य में इसके संबंध में बहुत उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कई व्यक्ति और संस्थाएँ योगशास्त्र के प्रसार का और शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं। इसलिए यह योग-दीप फिर एक बार प्रज्वलित हो उठा है। मन, बुद्धि, अहं और चित की सामर्थ्य मनुष्य की विशेषता है। वह अपनी पाँचों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति और बाह्य घटनाओं का अवलोकन कर सकता है और उन्हें आत्मसात भी कर सकता है। इसके कारण उसमें अलग-अलग प्रकार की अच्छी-बुरी वृत्तियाँ प्रकट होती हैं। इसका परिणाम यह भी होता है कि कई बार मनुष्य सत् और असत् को जानने की अपनी शक्ति का उपयोग न करके कुछ अन्य व्यवहार कर जाता है। ऐसी स्थिति में सुख या दुःख पैदा होता है। गलत वृत्तियाँ हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होती हैं।
इस शास्त्र में मानव में शारीरिक, मानसिक नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन करने की शक्ति तो है, साथ ही उसके अपने व्यक्तिगत सांस्कृतिक स्तर और पूरे समाज के सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने की क्षमता भी है। इसीलिए तो यह शास्त्र मानव जाति के लिए वरदान है। पिछली आधी शती में जनसामान्य में इसके संबंध में बहुत उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कई व्यक्ति और संस्थाएँ योगशास्त्र के प्रसार का और शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं। इसलिए यह योग-दीप फिर एक बार प्रज्वलित हो उठा है। मन, बुद्धि, अहं और चित की सामर्थ्य मनुष्य की विशेषता है। वह अपनी पाँचों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति और बाह्य घटनाओं का अवलोकन कर सकता है और उन्हें आत्मसात भी कर सकता है। इसके कारण उसमें अलग-अलग प्रकार की अच्छी-बुरी वृत्तियाँ प्रकट होती हैं। इसका परिणाम यह भी होता है कि कई बार मनुष्य सत् और असत् को जानने की अपनी शक्ति का उपयोग न करके कुछ अन्य व्यवहार कर जाता है। ऐसी स्थिति में सुख या दुःख पैदा होता है। गलत वृत्तियाँ हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होती हैं।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book